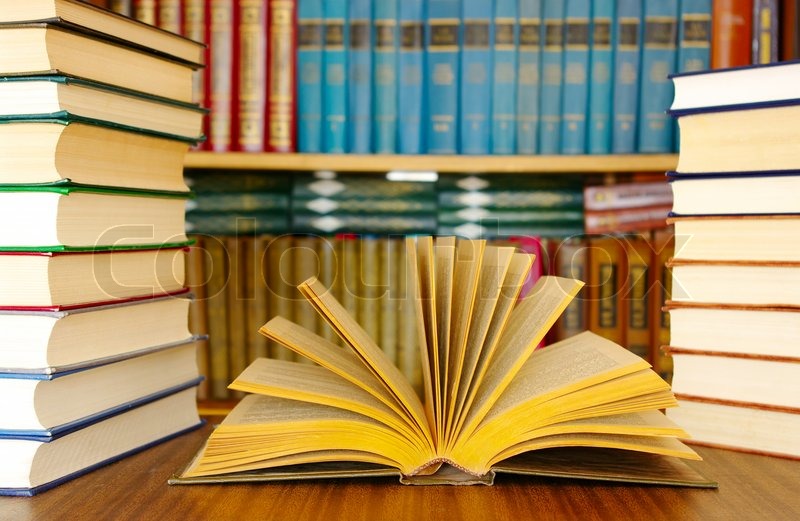अनुवाद के सिद्धांत
अनुवाद एक भाषा की बात को दूसरी भाषा में व्यक्त करने का नाम है। जिसकी उत्पत्ति अनु+वाद के संयोग से हुई है। जिसका अर्थ है
जब पर्याय की बात प्रबल हुई तो अन्य
भाषाओं में अनुवाद की प्रक्रिया भी तीव्र हुई। फलतः विद्वानों ने अनेक भाषाओं के
अनुवाद के दौरान होने वाली कठिनाईयों और सुलभता को आकंते हुए इसके लिए कुछ
सिद्धांत दिए हैं। जिन पर आगे चलकर विभिन्न आधारों पर अनुवाद सिद्धांतों को
प्रतिपादित किया गया। उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा नीचे की जाएगी।
अनुवाद संबंधी सिद्धांतों पर स्वतंत्र ग्रंथों का लेखन वस्तुतः
बीसवीं शताब्दी से आरंभ हुआ है। इसी शताब्दी के दौरान साहित्यिक और भाषा-वैज्ञानिक
पत्रिकाओं में अनुवाद पर लेखों का प्रकाशन आरंभ हुआ और अनुवाद संबंधी पत्रिकाएँ
आरंभ हुई। विभिन्न कालों में पश्चिम में अनुवाद को तरह-तरह से परिभाषित करने का
प्रयास किया गया है। कुछ परिभाषाएँ हैं—
जे.
सी. केटफोर्ट के अनुसार— “अनुवाद स्रोत भाषा की पाठ-सामग्री को लक्ष्य
भाषा के समानार्थी पाठ में प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है।”
सेंट
जेरोम के अनुसार – “अनुवाद में भाव की जगह भाव होना
चाहिए न कि शब्द की जगह शब्द।”[1]
अनुवाद सिद्धांत अनुवाद सिद्धांत मुख्यतः निम्न प्रकार के हो
सकते हैं
समतुल्यता का सिद्धांत
समतुल्यता का
सिद्धांत अनुवाद सिद्धांतों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कैटफोर्ड इस सिद्धांत के
प्रवर्तक माने जाते हैं। कैटफोर्ट का मानना था कि स्रोत भाषा की पाठ्यसामग्री को
लक्ष्य भाषा की सभ्यता में स्थापित करना ही अनुवाद है। इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र
में गंभीरता से विचार करते हुए योजना एवं समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
सूक्ष्मता से विचार करने पर ज्ञात होता है कि विभिन्न भाषाओं में शत-प्रतिशत समतुल्यता
संभव नहीं। अतः अनुवाद में भी उतनी समतुल्यता नहीं हो सकती। अच्छा अनुवाद मूल के
निकट हो सकता है मूल नहीं। यह तभी संभव है जब अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य
भाषा दोनों का अच्छा ज्ञान होता हो। समतुल्यता के लिए अनुवादक को अन्य विषय का भी पर्याप्त
ज्ञान होना चाहिए। यह अनुवादक का अत्यंत अपेक्षित गुण है। जिससे अनुवाद मूल के
निकट जाकर मूल की ही भांति प्रतीत हो सके।
व्याख्या का सिद्धांत
व्याख्या का
सिद्धांत पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण दोनों में ही अनुवाद को ही व्याख्या माना
गया है। जेम्स होम्स ने भी अनुवाद को व्याख्या ही माना है। अनुवादक को कुछ जगह
अनिवार्यता व्याख्या का सहारा लेना ही पड़ता है। भाषाओं की लोकोक्तियां, मुहावरें,
स्थानीय युक्तियाँ इत्यादि सामाजिक संदर्भ का शाब्दिक अनुवाद संभव नहीं हो पाता।
ऐसी स्थिति में अनुवादक को अनुवाद के लिए सिद्धांत का विनियोग करना पड़ता है।
व्याख्या से अनुवाद करने के लिए लक्ष्य भाषा वही अर्थ निकले इसके लिए पाद टिप्पणी
का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा यह है कि आवश्यकता से अधिक
व्याख्या होने पर अनुवाद अपनी सार्थकता खो देता है। अतः अनुवादक को विशेष सावधान
रहना चाहिए कि काव्य तत्व को स्पष्ट करने के लिए ही व्याख्या का प्रयोग करे न की
स्वयं की दक्षता को प्रदर्शित करने के लिए। उदाहरणतः AIIMS को करने पर स्पष्ट भाव व्यक्त
होते हैं। इसलिए इसकी व्याख्या ऑल इंडिया इंस्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या अखिल
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
कहना उपयुक्त रहा।
अर्थसंप्रेषण का सिद्धांत
भाषा-संवाद
अनुवाद की सार्थकता को यथावत बनाए रखने में अर्थ संप्रेषण की भूमिका अतुलनीय है। प्रायः
सभी भाषा वैज्ञानिक और अनुवाद चिंतक इस बात से सहमत हैं कि अर्थ अनुवाद का मुख्य तत्त्व
है। अर्थ संप्रेषित न होने पर अनुवाद निरर्थक हो जाता है। डॉ. जॉनसन का मत है—
‘अर्थ को
बनाएं रखते हुए किसी अन्य भाषा में अंतरण करना ही अनुवाद है।’ अनुवादक
को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सीमा में रहते हुए अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से
वह लेखक के निकट रहे। अनुवाद मूल की छाया होती है किंतु मूल नहीं। वस्तुतः अनुवादक
सदैव अनुवाद में कुछ जोड़ता और घटता रहता है। क्योंकि अर्थ के लिए शत-प्रतिशत
अनुवाद संभव नहीं। इसलिए हर अनुवादक यह प्रयास करता है कि वह श्रेष्ठ अनुवाद करके
मूल के निकट जा सके। मूल के निकट जाने वाला अनुवाद ही श्रेष्ठ समझा जाता है।
सांस्कृतिक संदर्भों के एकीकरण का
सिद्धांत
इस सिद्धांत को
सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मर्लिनो बख्शी ने प्रतिपादित किया है।
अनुवाद का सांस्कृतिक महत्त्व सर्वविदित है कि अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु है।
प्रत्येक भाषा की अपनी संस्कृति होती है। यही कारण है कि सांस्कृतिक पक्ष से
संबंधित अभिव्यक्तियों के अनुवाद में विशेष कठिनाई होती है। स्रोत भाषा और लक्ष्य
भाषा के सांस्कृतिक संदर्भों को भली-भांति समझकर अनुवाद करना उपयुक्त होता है।
मैलिनोवस्की मानते हैं कि अनुवाद संस्कृत संदर्भों का एकीकरण है। यही विचार
अंग्रेजी अनुवाद चिंतक देने है— वह मानते हैं कि
अनुवाद भाषाओं का अंतरण नहीं अपितु संस्कृतियों का अंतर है। इसलिए
अनुवाद सिद्धांत के अंतर्गत सांस्कृतिक संदर्भों का एकीकरण चिंतन अनुवाद के
सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। यही कारण है कि भारत विश्व-बधुंत्व की भावना को
साकार करते हुए एकीकरण की भावना पर बल देता है। अनुवाद के कारण ही आज संपूर्ण
विश्व एक ग्राम रूप में प्रतिष्ठापित होता जा रहा है।
निष्कर्षतः
अनुवाद सिद्धांत निरूपण यद्यपि इस शताब्दी की महत्त्वपूर्ण घटना है। किंतु अनुवाद
संबंधी विवेचन सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। पश्चिम में इसकी एक सुधीर परंपरा रही
है। बाईबल के अनुवाद के माध्यम से अनुवाद की प्रक्रिया और स्वरूप पर बहुत विचार
हुआ है। भारत में भी अनुवाद की परंपरा से अनुवाद के अन्य सूत्र मिले हैं। इस पूरे
विवेचन से स्पष्ट है कि अनुवाद के मुख्यतःउपर्युक्त सिद्धांत है। जिसमें व्याख्या
का सिद्धांत, अर्थ-संप्रेषण का सिद्धांत और संदर्भों के एकीकरण का सिद्धांत है।
अंततः अनुवाद विभिन्न विचारधाराओं को एक माला में मोती की भांति संग्रहित रूप में
प्रस्तुत करने की अतुलनीय कला है। अर्थात् अनुवाद की एक सूक्ष्म चर्चा पाश्चात्य क्षेत्र में मिलती है। भारत में
अनुवाद की परंपरा के सूत्र एक लंबे समय से विद्यमान है।
संदर्भ ग्रंथसूची
·
गुप्त अवधेश मोहन, अनुवाद विज्ञानः
सिद्धांत और सिद्धि, एक्सप्रेस बुक सर्विस, दिल्ली।
·
नवीन,देवशंकर, अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य,
प्रकाशन विभाग, प्रथम संस्करण, दिल्ली।
·
खन्ना, संतोष, अनुवाद के नये परिप्रेक्ष्य,
विधि भारती परिषद, दिल्ली, प्रथम संस्करण, दिल्ली।
·
सिंह, डॉ. रामगोपाल, अनुवाद विज्ञान,
शांति प्रकाशन, दिल्ली।
नाम- सुमन
कार्य- ज्वाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (शोधार्थी)
ईमेल आई डी- sumankumari10191@gmail.com
ब्लॉग- sumansharmahot.blogspot.com