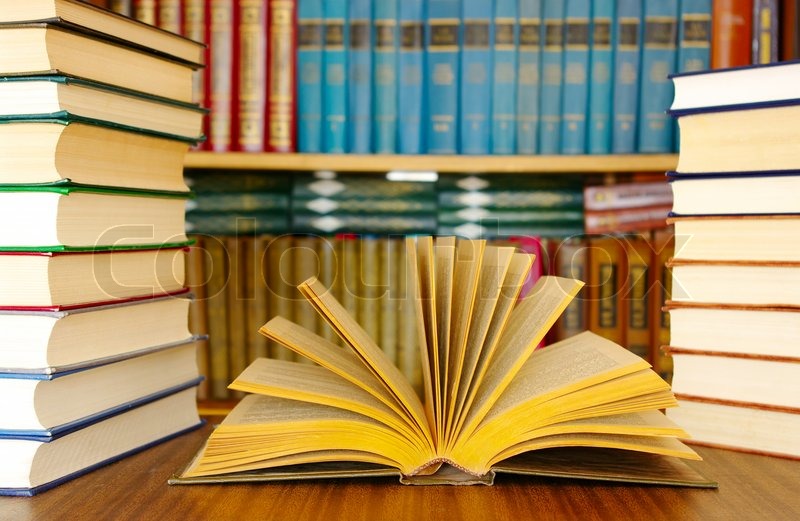नई शिक्षा नीति 2020-- संक्षिप्त विवरण
नई दिल्ली
कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति *(New Education Policy 2020)* को हरी झंडी दे दी है, *34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव* किया गया है। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल *निशंक* ने कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी, ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बडे़ स्तर पर सबकी राय ली गई है।
― नई शिक्षा नीति के तहत अब 5 वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा।
― बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।
― 9 वींं से 12 वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी, स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा।
― वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी।
― 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स एक साल में MA कर सकेंगे।
― अब स्टूडेंट्स को न M.Philहीं करना होगा, बल्कि MA के छात्र अब सीधे Ph.D कर सकेंगे।
पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जुटाई गई थी राय …।इस शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर राय ली गई थी। इसका अंदाजा इन आंकड़ों से सहज ही लगाया जा सकता है। इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई थी।
हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है।
हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं।सु सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नैशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा। देश में अभी 45 हजार कॉलेज हैं।
सरकारी, *निजी*, *डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम
हायर एजुकेशन सेक्रटरी अमित खरे ने बताया, नए सुधारों में टेक्नॉलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहां डीम्ड यूनविर्सिटी*, *सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंडअलोन इंस्टिट्यूशंस के लिए अलग-अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे।
*कक्षा10वीं में नहीं होंगे बोर्ड एग्जाम, पढ़ें नई शिक्षा नीति की 10 बड़ी बातें
*नई दिल्ली* : मोदी कैबिनेट ने आज नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला किया, शिक्षा नीति में ये बदलाव 34 साल बाद हुआ।नई शिक्षा नीति से जुड़ी दस बड़ी बातें।
― 5वीं तक कम से कम और आठवीं और उससे आगे भी मुमकिन हुआ, तो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ना होगा, यानि कि हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होंगे।
― अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है। लेकिन अब ये *5+3+3+4* के हिसाब से होगा, यानि कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पांचवी तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौंवी से 12 वीं तक आखिरी हिस्सा होगा, बारहवीं में बोर्ड की परीक्षा होगी । लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव होंगे।
― छात्र अपनी मर्जी और स्वेच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे, तो उसे ये विकल्प होगा। दसवीं की परीक्षा और उसके स्वरूप को लेकर अभी असमंजस्य की स्थिति है। वोकेशनल पाठ्यक्रम कक्षा छठी से शुरू हो जाएंगे।
― बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और उसमें रटकर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा।
― बच्चा जब स्कूल से निकलेगा, तो ये तैय किया जाएगा कि वो कोई ना कोई स्किल लेकर बाहर निकले।
― बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा, अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता है लेकिन नई शिक्षा नीति में तीन हिस्से होंगे।
*पहला*
बच्चा अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा,
*दूसरा*
उसके सहपाठियों से होगा और
*तीसरा* अध्यापक के जरिए।
― ग्रेजुएट कोर्स में अब 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री मिलेगी, अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी, 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है।
― हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, उनके लिए MA एक साल में करने का प्रावधान होगा।
― नई नीति स्कूलों और एचईएस दोनों में बहु-भाषावाद को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय पाली संस्थान, फारसी और प्राकृत, भारतीय अनुवाद संस्थान और व्याख्या की स्थापना की जाएगी।
*शिक्षा नीति में बदलाव बहुत बड़ा व बहुत बढ़िया निर्णय है*, *ये कदम शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ेंगे ...।