भारतेन्दु के अनूदित एवं मौलिक नाटक
भारतेन्दु का संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजी और बांग्ला
आदि भाषाओं पर पर्याप्त अधिकार था। सच्चे नाटककार के नाटक सदैव से युग का
प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने राजनैतिक चोलों की चोटों से युक्त यथार्थवादी
शैली का आदर्श रूप मुद्राराक्षस का पूर्ण अनुवाद करने मे ही श्रेयष्कर
समझा।
रत्नावली भारतेन्दु का अनुवाद के क्षेत्र में प्रारम्भिक और सफल प्रयास है
जिसमें पाखण्ड-विडम्बन में भावों का द्वंद बड़े मनोवैज्ञानिक ढ़ंग से
चित्रित हुआ है। धनंजय विजय नाटक के लेखक ने पद्य शैली अपनाई वहीं
भारतेन्दु ने केवल पद्य शैली की सत्ता स्थापित की। उनका दुर्लभ बंधु
शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेन्ट आफ वैनिस का सफल अनुवाद है। विद्यासुन्दर
भारतेन्दु की रुपान्तरित रचना है। यह बंग देश के नाटक विद्यासुन्दर की छाया लेकर
निर्मित हुआ है। भारत जननी बंग्ला के भारतमाता का अनुवाद है। “सत्य हरिशचन्द्र”
भारतेन्दु की सफल एवं प्रतिनिधि मौलिक रचना है। सती प्रताप भारतेन्दु की
अपूर्ण कृति है इसमें सावित्री-सत्यवान के पौराणिक कथा इतिवृत्त को ग्रहण किया है।
प्रेमजोगिनी काशीनगर के अधर्मरत ठेकेदारों व भारतीय धार्मिक पाखण्डों का
प्रतिछलन रूप दिखाया है। वहीं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में भी धर्म की
आड़ में दुराचार करने वाले तथा मांसभक्षियों मिथ्याचारी, पाखण्डियों की खिल्ली
उड़ाई गई है। विषस्यविषमौषधम् में बड़ौदा के राजा मल्हार राव के कुशासन का
वर्णन है। भारत दुर्दशा प्रतीकात्मक दुखांत नाटक है वहीं भारत जननी
में पराधीन भारतीयों दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण है। नीलदेवी में
स्त्री की ओजस्वी छवि का चित्रण है।
भारतेन्दु ने अनुवादों के मूल में निहित मन्तव्यों व सामयिक, उपयोगिता का
स्पष्टीकरण, भूमिकाओं व आरम्भिक राष्ट्र समर्पण से हो जाता है। इन्होंने पात्र और
कथा का भारतीयकरण किया है। भारतेन्दु ने राष्ट्रप्रेम, राष्ट्र कल्याण एवं जनजागृत
नवचेतना को आधार संस्कृत, पारसी, अंग्रेजी से प्रभावित होकर ग्रहण किया है जिसका
जीवांत उदाहरण मर्चेन्ट आफ वेनिस का दुर्लभबन्धु है।
भारतेन्दु का जन्म 9 सितम्बर 1850 को और मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हुई।
इन्होंने अपने नाटक नामक निबंध में अपने 19 नाटकों का जिक्र किया
है। जिसमें मौलिक और अनूदित दोनों सम्मिलित हैं। भारतेन्दु के नाटक लेखन का
श्रीगणेश 1868 ई. से हुआ। सन् 1868 से 1885 ई. तक अपने अत्यंत व्यस्त जीवन के शेष 17
वर्षों में अनेक नाटकों का सृजन कर अभिनेय को भी प्रेरित किया।
काशी में भारतेन्दु के संरक्षण में नेशनल थियेटर की स्थापना हुई। जिसमें
उन्होंने अपने मौलिक व अनूदित नाटकों का अभिनेय किया।
भारतेन्दु हरिश्चंद के अनूदित नाटकों में रत्नावली (1868), धनंजय विजय (1873), पाखण्ड विडम्बन
(1872), मुद्राराक्षस (1875), कर्पूरमंजरी (1876), दुर्लभबंधु (1880),
विद्यासुन्दर आदि अनूदित
नाटक हैं जो संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी से अनूदित हैं।
विद्यासुन्दर रूपान्तरित नाटक है।
भारतेन्दु के मैलिक नाटकों में कथावस्तु की अनेकरूपता, विविधता एवं मौलिकता के
दर्शन होते हैं। विचार और भावपक्ष की दृष्टि से इनमें तत्कालीन अधिकांश
विकासोन्मुखी नई प्रवत्तियां, विशेषकर राष्ट्रीयता और समाज-संस्कार आदि प्राण रूप
में समाई हुई है। भारत दुर्दशा और भारत जननी में देशप्रेम, सत्यहरिशचन्द्र
में सत्यप्रेम, सतीप्रताप में पतिप्रेम, चन्द्रावली में
ईश्वरोन्मुखी प्रेम तथा सत्य हरिशचन्द्र नाटक में इनके प्रकृति प्रेम का परिचय
मिलता है।
भारतेन्दु ने नाटकों में आत्महीनता के स्थान पर स्वाभिमान और आत्मगौरव की बात
की है। भारत दुर्दशा के आरम्भ में योगी का गान इसी भावाशय का द्योतक है।
कार्यव्यापार और कौतूहल अधिकांश रचनाओं के अनिवार्य अंग हैं। सत्यहरिशचन्द्र,
नीलदेवी, अंधेर नगरी तथा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में तो कार्यगति
अत्यंत तीव्र है। प्रेम जोगिनी अपूर्ण में भी कार्यव्यापार एवं सजीवता की दृष्टि
से सफल रचा है।
चन्द्रावली में कथा वैचित्य का
अभाव होते हुए भी वस्तु संघटन बड़ी सुन्दरता से हुआ है। भारत दुर्दशा अन्यापेदशिक
नाटकों की कोटि की रचना होते हुए भी वस्तु संगठन की दृष्टि से सफल है। चन्द्रावली
में कृष्ण की प्रशंसा के साथ प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना का प्रयोग है।
भारतेन्दु ने रिश्वतखोरी, शोषक अंग्रेजों और भ्रष्ट पुलिस वालों पर व्यंग्य
किया है। इन्होंने नाटकों में मनोरंजन और उपदेश दोनों की प्रक्रिया रखते हुए नाटक
रचे हैं।
भारतेन्दु के अनुवादों की भाषा में संवाद सशक्त एवं गीत और पद्य अच्छे हैं।
इनमें प्रयुक्त भाषा भी पौढ़, सजीव, व्यंजनापूर्ण है। कर्पूरमंजरी में विचक्षणा
और विदूषक का संवाद अत्याकर्षक एवं सजीव हुआ है। मुद्राराक्षस अनुवाद की
भाषा सबसे अधिक प्रांजल है। डा. सोमनाथ गुप्त के अनुसार – मुद्राराक्षस तो हिन्दी
गद्य की व्यंजना शक्ति और भारतेन्दु की गद्य दक्षता का निर्विवाद उदाहरण है।
भारतेन्दु ने अधिकांश नाटकों को सरल, दृश्य विधान और यथार्थवादी शैली में लिखा
हैं। चन्द्रावली सरस प्रेमविधान नाटिका शैली में लिखा है। विषस्यविषमौधम
भाण शैली में लिखा गया प्रहसन है। अंधेर नगरी व्यंग्य प्रधान वर्णन
शैली का प्रहसन है। भारत दुर्दशा प्रतीकात्मक दुखांत नाटक
है जो विश्लेषणात्मक शैली में है। नीलदेवी गीतिरूपक शैली
में है। वहीं प्रेम जोगिनी गर्भांक शैली में रचित नाटक है।
भारतेन्दु ने अपने नाटकों के माध्यम से हिन्दी नाट्यकला को नवीन, स्वस्थ,
मौलिक एवं स्पष्ट रूपरेखा प्रदान की है। वह अपनी नाट्यशक्ति और सामर्थ्य के बल पर
नवोत्थान और पुरोधा नाटककार बने हैं। उन्होंने खड़ी बोली को स्वभाविक एवं निश्चित
रूप दिलाने, गद्य, की प्रधानता को बढ़ाने तथा नाटक को अनिवार्य गुण अभिनेयत्व के
साथ विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
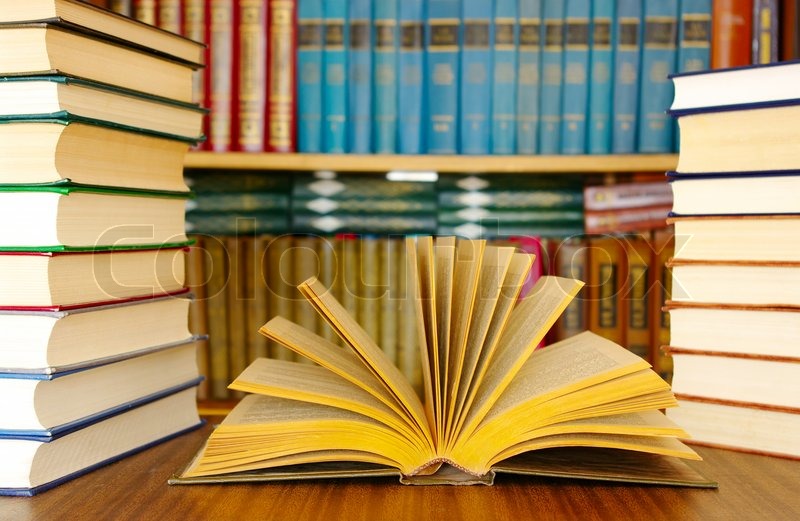
very nice
ReplyDeleteबढ़िया
ReplyDeleteबहुत-बहुत आभार मैम।
DeleteGood
ReplyDeleteVery nice
ReplyDeleteThank so prof. Venudhar Routiya sir.
ReplyDeleteIf want some suggestions plz tell me sir. I am very greatful you.🙏🙏🙏
Nice
ReplyDeleteNice
ReplyDeleteथैंक यू ऑल
ReplyDeleteNice
ReplyDeleteThankyou
ReplyDeleteGood information
ReplyDelete